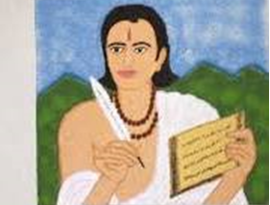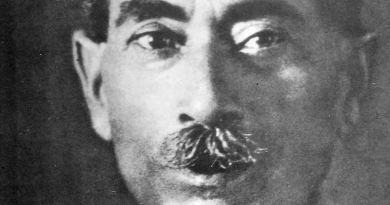गढ़वाल के लोकगीत – डॉ0 माधुरी बड़थ्वाल
उत्तराखंड का स्मरण करते ही स्मृतिपटल पर उभर आती है हिमालय की रमणीक हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियॉ, फल, फूलों से भरे हुये पहाड़, भॉति-भॉति के पक्षी और उनका मधुमिश्रित स्वर, पवित्र नदियॉ, सीड़ीनुमा खेत उनमें विचरते पशु, शैल बालायें, शांत, स्वच्छ वातावरण में दूर-दूर से आती आवाजें, ऐसी मधुर कि हर स्वर मधु मिश्रित ! चाहे वह पशु-पक्षी का हो, किसी साज़ या फिर सास और मॉ या सगे संबंधियों द्वारा अपनी बहू- बेटी या संबंधियों को पुकारने का। चारों ओर संगीतमय वातावरण। सृश्टि रचना की सुप्रभात बेला में सर्व प्रथम समुद्र के गर्भ से जिस स्थान पर निराकार ब्रह्म का साकार रूप में आविर्भाव हुआ वेद-पुराणों में उसी को हिमवंत नाम से संबोधित किया जाता है। महाकवि कालीदास के देवात्मा हिमाद्रि-स्थित केदार मानसखंड की प्राचीनता के संदर्भ में कहा जाता है कि भगवान षिव ने उद्घोश किया कि-’’जैसे मैं प्राचीन हूं उसी प्रकार केदारखंड भी प्राचीन है। जब मैं ब्रह्ममूर्ति धारण कर सृश्टि रचना में प्रवृत्त हुआ, तब मैं ने इसी स्थान पर सर्व प्रथम सृश्टि रचना की।’’ वर्तमान में इसी स्थान को उत्तराखंड की संज्ञा से विभूषित किया गया।
वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल भूभाग को प्राचीन काल से केदारखंड, बद्रिकाश्रम, उत्तराखंड, स्वर्गभूमि, तपोभूमि या हिमवंत नाम से जाना जाता रहा है। इस क्षेत्र विषेश का गढ़वाल नाम पंद्रहवीं षताब्दि में परिवर्तित किया गया। उतुंग पर्वत श्रृंखलायें हमेषा वर्फ से ढकी रहती हैं। बंदरपूॅछ पर्वतमाला भागीरथी, यमुना सहित अनेक नदियों का पालन-पोशण करती है। पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी पर साथ-साथ बहती हुई अपना घुमावदार मार्ग बनाती हुई ये गंगा, यमुना की सहायक नदियॉ संगम बनाती हुई गंगा मॉ के साथ मैदानी भाग में प्रवेष करती हैं। गढ़वाल के भूभाग में चौखंबा, सतोपंथ, नर-नारायण, मंदाकिनी, तुंगनाथ और रामणी आदि अनेक छोटी बड़ी पर्वत श्रृंखलायें हैं जिनके षिखरों पर श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदार नाथ, गंगोत्री, यमनोत्री पावन पवित्र धाम हैं। भगवान षिव-षैलजा का वास कैलाष है। इन्हीं अनेक हमेषा हिमाच्छादित रहने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित तालों और हिमानियों से भागीरथी, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, धौळी गंगा सहित अनेक पावन नदियों का उद्गम हुआ। कहा जाता है गढ़वाल की यह पावन पवित्र भूमि देवताओं को बहुत प्रिय है। इसीलिये यह ऋशि मुनियों की तपोभूमि है। इस पुण्य भूमि में देवताओं का निवास है।
लोकगीत जो लोक संस्कृति के सबसे पौराणिक आख्यान हैं, इतिहास, भूगोल, रीति रिवाज़, रहन सहन, खान-पान, बोली- भाशा सब हमारे पूर्वजों ने बड़ी सहजता से इन्हीं में अवगुंठित कर सहेजा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली परम्परागत मौखिक सारगर्भित षब्दों की वह संगीत बद्ध रचना, जिसमें जन-जन की खट्टी-मीठी सम्वेदनाओं का मर्म हो लोकगीत कहलाती है। लोकगीत किसी व्यक्ति विषेश का न होकर जन साधारण की धरोहर है। यहॉ के थड्या या चॉछड़ी लोकगीत में कहा गया है कि -जब देवताओं को धरती पर सब जगह अषुद्ध वातावरण दिखाई दिया तो उन्होंने यही कहा कि- उत्तराखंड की भूमि सबसे पवित्र भूमि है वहीं चलते हैं। यथा :-
जै जै बदरीनाथ जी झमको। जै जै बदरीनाथ जी झमको।
चल चल द्यवताओं जी झमको। चल चल द्यवताओं जी झमको
उतराखॅूट जौला जी झमको। उतराखॅूट जौला जी झमको।
देसन की भूमी जी झमको। असुध ह्वेग्याई जी झमको।
उतराखॅूट भूमि जी झमको। पबित्र बतूनी जी झमको।
अर्थात- देश परदेश की अधिकतर भूमि अपवित्र हो गई। चलो सभी देवताओं ! उत्तराखंड में चलते हैं। उत्तराखंड की भूमि सबसे पवित्र भूमि है। सभी देवता एक साथ मिलकर पवित्र भूमि उत्तराखंड की ओर यात्रा पर चल पड़ते हैं।
इसी तपोभूमि में पुण्य ग्रंथों की रचना हुई है। मानव सभ्यता के पहले पायदान से ही साधारण लोक वासियों ने ऋशि मुनियों की वाणी सुनकर आत्मसात कर सृश्टि की रचना से लेकर ही अनेक अत्यंत पौराणिक आख्यान यहॉ के लोकगीतों में वर्णित किये हैं, जो लोक संस्कृति की धरोहर हैं। माता पार्वती का मायका, जन्म स्थल। भगवान षिव का निवास, चारों धाम अवस्थित हैं। इसीलिये इस देवभूमि की लोक संस्कृति अधिकतर आध्यात्म और प्रकृति की गोद में पली-बढ़ी है। किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक परम्परा में लोक संगीत की अहम भूमिका होती है अतः लोक संगीत ही लोक संस्कृति का सच्चा संवाहक है।
लोक संगीत लोक जीवन का प्रतिबिम्ब होता है। लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी, आम जन द्वारा की गई, लोक जीवन की, संगीतमय अभिव्यक्ति की, सांस्कृतिक विरासत की मौखिक परंपरा है। लोक गीत व्यक्ति विषेश के न हो कर जन सामान्य द्वारा रचित वर्षों पुरानी लोक परंपरा की धरोहर होते हैं। व्यक्ति विशेष की रचना सुगम संगीत के अंतर्गत आती है। सुगम संगीत में गीत, भजन या ग़ज़ल के साथ रचनाकार का नाम हमेषा जुड़ा रहता है। हज़ारों वर्श पुराने ग्रंथों के रचनाकार का नाम हमेषा से जुड़ा हुआ है, जैसे उदाहरण स्वरूप श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास युगों तक अमर रहेंगे जब तक ये धरती माता है।
गढ़वाल का लोक संगीत भाशा, भाव और संगीत की दृश्टि से अत्यंत समृद्ध है, आवष्यकता है तो बस उसे समझने की और सुरक्षित कर संरक्षित करने की। संस्कृति इसी लोक संगीत में रचती बसती है, चिरायु रहती है, इसीलिए यदि माना जाय कि लोक संगीत लोक संस्कृति की आत्मा है तो अतिषयोक्ति न होगी। उत्तराखंड में लोक संगीत के संरक्षण और संवर्द्धन में देवभूमि की नारी षक्ति की अहम भूमिका है। एक गॉव की बेटी विवाह के उपरांत दूर ससुराल गई साथ ले गई अपने लोक संस्कार, अपना लोक संगीत ! और फिर साथ लेजाई गई कला को समाज में सरसब्ज़ किया। लोक संगीत के अंतर्गत भी गायन, वादन और नृत्य संगीत की इन तीनों कलाओं का समावेष होता है। नृत्य वादन के और वादन गायन के आधीन है। गायन में लोकगीत, वादन में लोक वादन और नृत्य के अंतर्गत लोकनृत्य आते हैं।
गढ़वाल के लोकगीतों को जाति वर्ग के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। क्योंकि लोकगीत किसी एक व्यक्ति की सम्पति बनकर नहीं रहते। इनमें जन-जन की आत्मा बसती है। मैं से नहीं ंहम द्वारा रचे बसे हैं इसलिये लोकगीत हमारी धरोहर हैं। स्वर, लय, छंद बद्ध गढ़वाली लोकगीतों के विभिन्न प्रकारों को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता हैः-
1- धार्मिक
2- सामाजिक
हरेला लोकपर्व समारोह में लोकगीत का मंच प्रदर्शन
धार्मिक लोकगीत- यूं तो धार्मिक लोकगीत भी सामाज के ही हैं, किन्तु इनके गायन की एक नियम और आस्था बद्ध परंपरा है। जागर गायक, जो जागरी कहलाते हैं, जागर लोक गाथाओं को विधि विधान से गाते हैं। इनमें जो वृहद काव्य गाथायें होती हैं, जागर गाथा या अन्य लोक गाथा के, उनके कुछ सरल जनसाधारण के ग्राह्य अंष, थड्या या अन्य लोकगीतों के रूप में भी गाये जाते हैं। नैसर्गिक धुनों में सृजित काव्य जो जन, मन, रंजन करें, जो आम जन को पुलकित करें, आम जन उस लोक गाथा के अंष को मनोरंजन के लिये स्वच्छंद होकर आत्मसात कर लेता है। जागर षैली की इन लोक गाथाओं का वर्गीकरण इस प्रकार हैः-
1- देवी, देवताओं के जागर लोकगीत।
2- रख्वाळी, झाड़ो-ताड़ो, हंत्या के जागर लोकगीत।
3- सैद्वाळी।
4- भूतप्रेत, ऑछरी के मनौती लोकगीत।
5- पॅवाड़ा, भड़ैलो, रॉसो।
सामाजिक लोकगीत- जन सामान्य द्वारा स्वछंदता पूर्वक गाये जाने वाले लोकगीतों को सामाजिक लोकगीतों की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि मन के भावों को व्यक्त करने का सबसे सुलभ माध्यम है गाना या रोना ! जो सबको आता है। ये अलग बात है कोई प्रदर्षित करता है, कोई मन में रखता है। लोक गीत सबकी आत्मा से जुड़े होते हैं इसलिये इनमें सब षामिल होते हैं। सामाजिक लोकगीतों का वर्गीकरण इस प्रकार है :-
1- संस्कार लोकगीत मॉगळ।
2- ऑगन के लोकगीत – थड़्या, चौंफुला, ऋतु संदर्भित नृत्य प्रधान लोकगीत और बालगीत।
3- ऋतु प्रधान लोकगीत- चैती पॅसारा, बारामासा, झुमैलो, बसंत, ग्रीश्म, वर्शा, षरद, षीत ऋतु संदर्भित।
4- तीज त्योहार, मेले संदर्भित लोकगीत- होली, बाजूबंद, चॉछड़ी, छोपती, छपेली, फौंफती, छूड़ा, तॉदी, नाटी, हारुल, धूपछाड़ा, लामण आदि।
5- पियोग या करुणरस प्रधान लोकगीत- खुदेड़, आलाप प्रधान न्योली, आलाप प्रधान झुमैलो लोकगीत।
6- हास्य-व्यंग्य प्रधान लोकगीत।
7- घटना प्रधान लोकगीत।
8- देव यात्रा प्रधान लोकगीत, निर्गुण।
9- चखुल्या और विकास लोकगीत।
10- व्यवसायिक लोकगीत- बाद्दी लोकगीत, हुड़क्या।
11- लोक गाथायें।
- डॉ0 माधुरी बड़थ्वाल, संगीत संयोजिका/निदेशका